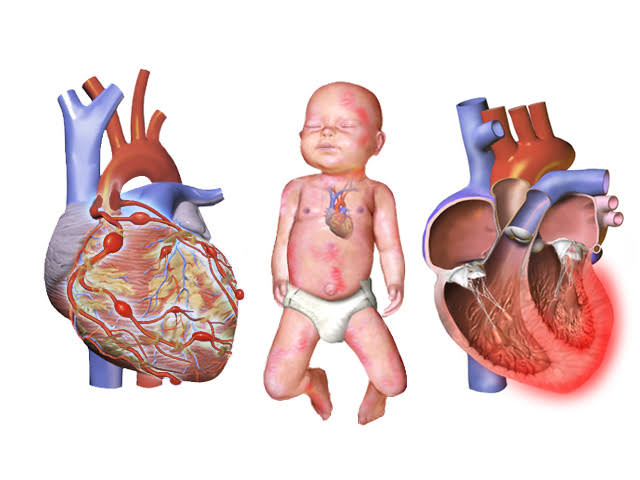क्वारंटाइन कॉन्सपिरेसी के लिए उत्तम माहौल देता है। जब लोग घरों में लगातार बन्द होते हैं , तब वे समाज से कट जाते हैं। वे केवल उस / उनकी सुनते हैं , जिसपर वे सबसे अधिक भरोसा करते हैं। यह भरोसा परिवार के किसी ख़ास शक्तिशाली व्यक्ति पर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति धर्मगुरु हो सकता है , राजनेता भी। ऐसे लोग जो बुरे-से-बुरे समय में भी चेहरे पर शिकन न लाएँ। इस तरह बात करें कि उनके पास महाप्रलय का भी समाधान है। ऐसे ही लोग महामारियों के समय ढेर सारे लोगों के महानायक बने रहते या बन जाते हैं।
जो जितना डरा हुआ है , वह उतना आक्रामक होगा। जो आक्रामक होगा , वह कॉन्सपिरेसी से और अधिक चिपकेगा। जितना कॉन्सपिरेसी में विश्वास , उतना भय का विकास। जितनी भयवृद्धि , उतनी आक्रामकता में भी वृद्धि। जितनी अधिक आक्रामकता , उतना कॉन्सपिरेसी से और अधिक चिपकाव। कॉन्सपिरेसी-भय-आक्रामकता के इस चक्र का चलते जाना।
आक्रामकता हद दर्ज़े की स्वार्थी है। वह करुणा से दूर-बहुत दूर चली जाती है। व्यक्ति का आक्रामक होना केवल वैचारिक बात नहीं है। आक्रामकता ढेरों आचार-सम्बन्धी बदलाव लाती है। ऐसे ही लोग खाने-पीने के सामानों की जमाखोरी करते हैं , अफ़वाहें फैलाते हैं। इसी प्रकार के लोग दोषारोपण के लिए बलि-के-बकरे तलाशते हैं , उनके मत्थे सारा किया-धरा मढ़ देते हैं। इन लोगों में सामाजिक समानुभूति बहुत कम होती है , ये केवल अपने ( या बहुत हुआ तो अपने परिवार ) के बारे में सोचते हैं। जीवन को पूँजी मानकर ये डरे हुए आक्रामक लोग कॉन्सपिरेसीमय होकर ही महामारी का दौर काटते हैं।
कॉन्सपिरेसी में जीने वाला हमेशा धार्मिक व्यक्ति हो , ज़रूरी नहीं। वह धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है। सेक्युलर होना आपको साइंटिफिक टेम्पर नहीं देता। सेक्युलरिज़्म धर्मों के प्रति समभाव या उदासीनता रखने को कहते हैं। यह एक सामाजिक सोच है , जिसमें आप कई बार तार्किकता को एकदम किनारे लगा देते हैं। कोई बुरा न मान जाये , इसलिए तर्क ही न करो। सब ख़ुश रहें , बुरा न मानें। लेकिन तर्क का आह्वान न करने से तर्क करने की क्षमता कमज़ोर पड़ती जाती है। फिर ऐसे अतार्किक सेक्युलर लोग विज्ञान से दूर हटते हुए सेक्युलर कॉन्स्पिरेसियों के जाल में फँस सकते हैं। ध्यान रहे : वैज्ञानिक सोच के मामले में समभाव या उदासीनता नहीं रखी जा सकती , वहाँ तर्क का पक्ष लेना ही पड़ता है। ऐसे में कोई भी ऐसी ख़बर जिसमें राजनीतिक या आर्थिक शक्तिशालियों की गुटबाज़ी शामिल हो , उसमें भी कॉन्सपिरेसी के बीज पड़ सकते हैं।
जिस समस्या पर व्यक्ति का ज़ोर नहीं चलता , उससे परेशान होकर वह अपने स्थूल नायक की सुनता है। नायक-वायक की अनुपस्थिति में अनेक बार अपनी राजनीतिक विचारधारा को ही नायक बना लेता है। उसके चश्मे से महामारी के सापेक्ष हर शक्तिशाली व्यक्ति को देखने लग जाता है। शक्तिशालियों की खेमेबाज़ी तो पैंडेमिक-काल में चल ही रही है। अमेरिका की अमुक पार्टी दूसरी पार्टी पर दोष लगा रही है। अमुक सरकार दूसरी सरकार पर। अमुक देश के लोग दूसरे देश के लोगों पर। एक ही देश के अमुक लोग दूसरे लोगों पर। इन सबमें बड़े उद्योगपति भी सायास / अनायास शामिल हैं , अनेक डॉक्टर-वैज्ञानिक भी। इतने आरोप, इतने प्रत्यारोप , इतनी बातें और इतने विरोधाभास कि व्यक्ति डरते-डरते अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है।
उपाय क्या है ? वही जिसे घर का कोई भी विवेकवान् बड़ा-बूढ़ा आसानी से बता देगा। उस पर बात या चर्चा करो , जिसे बदल सकते हो। जिस पर बस नहीं , उसपर बात करने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारे प्रयास तुम्हारी सीमा हैं। बाक़ी आरोप-दोष-कॉन्सपिरेसी-षड्यन्त्र केवल ख़याली जुगाली। चाहे जितना चबाते रहो : सीआईए या एमआई श्वेतपत्र तो लाकर तुम्हें देंगी नहीं। और दे भी देंगी, तो क्या सच ही होगा वह ?
व्यक्तिगत-परिवारगत-समाजगत सकारात्मकता के अलावा बाक़ी ख़बरों का प्रसार केवल भय और आक्रामकता का माहौल बनाना है। डर भीड़ को खेमों में लामबन्द करने का सबसे आसान तरीक़ा है। इससे व्यक्ति को बड़ी आसानी से भीड़ में बदला जा सकता है। भीड़ समाज नहीं है। भीड़ और समाज में उतना ही अन्तर है , जितना पत्थरों के ढेर और पत्थर की दीवार में। दीवार में निर्मिति निहित है , ढेर में ध्वंस बैठा है।
और इस माहौल वाली भीड़ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है , यह तो सभी जानते हैं।